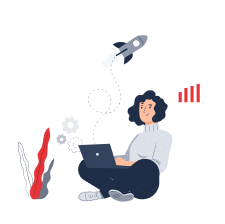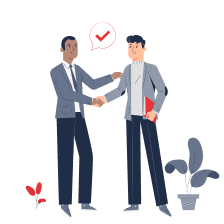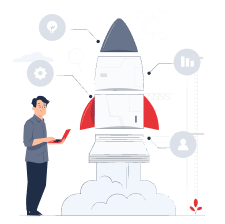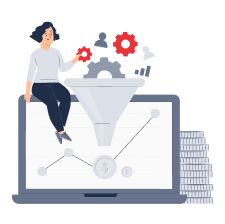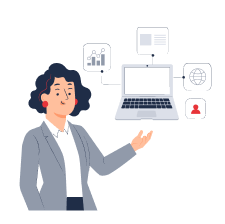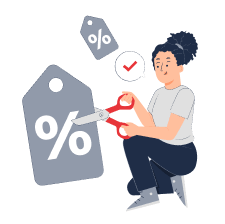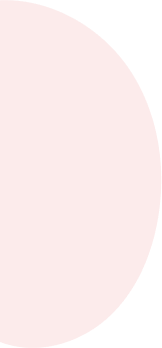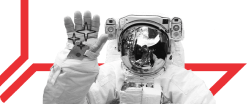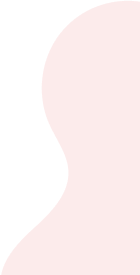इम्पोस्टर सिंड्रोम

इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है
इम्पोस्टर सिंड्रोम - एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर पाता और इस वजह से आत्म-संदेह महसूस करता है। आसान शब्दों में कहें तो, व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे उसने जो कुछ भी हासिल किया है, वह वास्तव में उसकी काबिलियत या मेहनत की वजह से नहीं है, बल्कि वह महज़ एक संयोग या किस्मत का साथ था। उसे लगता है कि वह अपने क्षेत्र का असली पेशेवर नहीं है, और जितना सम्मान या सफलता उसे मिली है, वह उसका हकदार नहीं है, जबकि उसके जैसी उपलब्धियों वाले अन्य लोगों को वह योग्य मानता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक तरह का मनोवैज्ञानिक भ्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में अनुचित और नकारात्मक सोच रखता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम में व्यक्ति को बार-बार नकारात्मक विचार आते हैं और उसमे नकारात्मक भावनाए पैदा होती हैं, जैसे कि: असली रूप में सामने आने का डर, यह चिंता कि लोग उसे धोखेबाज़ समझेंगे, लगातार तनाव और चिंता, असफलता को स्वीकारने में कठिनाई, ख़ुद की अत्यधिक आलोचना, इत्यादि। यह सब उस डर से पैदा होता है कि लोग अगर उसे "जैसा वह वास्तव में है" देख लेंगे, तो निराश हो जाएंगे।
इम्पोस्टर सिंड्रोम को एक मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में पहली बार 1970 के दशक में अमेरिकी मनोविज्ञान प्रोफेसर पॉलिन क्लैन्स और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुज़ैन इमेस ने वर्णित किया था। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उन्होंने इस सिंड्रोम की पहचान उन महिलाओं से बातचीत के दौरान की, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी आत्म-सम्मान की समस्याओं से जूझ रही थीं। इसी वजह से शोधकर्ताओं को लंबे समय तक यह विश्वास रहा कि इम्पोस्टर सिंड्रोम केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। आज भी, आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं इस सिंड्रोम से पुरुषों की तुलना में 2-3 गुना ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हालांकि, आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि यह सिंड्रोम वास्तव में दोनों लिंगों को प्रभावित करता है। आंकड़ों में यह असंतुलन इस कारण है कि पुरुष अक्सर अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार नहीं करते और आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद लेने में हिचकिचाते हैं। इस विषय पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 62% ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य बौद्धिक श्रम से जुड़ा है, इम्पोस्टर सिंड्रोम का अनुभव कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यह कोई दुर्लभ स्थिति नहीं है।
उत्पत्ति और विकास के कारण
इम्पोस्टर सिंड्रोम क्यों पैदा होता है? सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि भले ही इसके नाम में "सिंड्रोम" शब्द शामिल है, यह कोई मानसिक विकार नहीं है और न ही मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर विचलन। जैसा कि पहले बताया गया था, यह ज्यादातर एक आंतरिक विकृति और नकारात्मक विश्वास प्रणाली है, जो व्यक्ति के भीतर कुछ अप्रिय अनुभवों या विशिष्ट परवरिश की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप विकसित होती है - ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर दूसरे व्यवहारिक पैटर्न बनते हैं। दूसरे शब्दों में, यह नकारात्मक सोच का एक ऐसा तरीका है, जो समय के साथ व्यक्ति के भीतर बैठ जाता है, और व्यक्ति ख़ुद पर विश्वास करना छोड़ देता है, भले ही उसके पास स्पष्ट रूप से सफलता के प्रमाण हों।
इस प्रकार, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम बचपन से ही इंसान के जीवन में अपना स्थान बनाने लगता है, और इसके पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:
-
अधिक सफल सिबलिंग: जब माता-पिता हमेशा किसी और बच्चे (जैसे भाई, बहन, रिश्तेदार या किसी परिचित) को उदाहरण के रूप में पेश करते हैं - जो "ज्यादा काबिल, ज्यादा होशियार, ज्यादा ऐक्टिव" होता है - तो बच्चे के मन में यह आदत बन जाती है कि वह खुद की तुलना खुद से नहीं, बल्कि दूसरों से करने लगता है। जबकि स्वस्थ आत्ममूल्यांकन के लिए व्यक्ति को खुद की तुलना अपने पिछले रूप से करनी चाहिए।
-
अत्यधिक प्रशंसा: जब माता-पिता बच्चे की उपलब्धियों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन उसकी गलतियों पर काम नहीं करते, तो बातचीत का केंद्र बिंदु केवल प्रशंसा और तारीफ बन जाता है। अगर बच्चे को बार-बार यह कहा जाए कि वह "बहुत होशियार", "अद्वितीय", या "सबसे बेहतर" है, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस विकसित हो सकता है। लेकिन असल जीवन में जब वह विफलताओं से टकराता है - और चूँकि बचपन में उसे असफलता को स्वीकारना नहीं सिखाया गया होता - तो वह खुद की आलोचना करने लगता है, खुद को संदेह की नजर से देखने लगता है, और आत्मविश्वास खो देता है, भले ही वह उस काम को करने में वास्तव में सक्षम हो।
-
थोपे गए लक्ष्य: जब माता-पिता बच्चे में वे इच्छाएँ या रुचियाँ डालते हैं, जिन्हें वे खुद पूरा करना चाहते थे, और बार-बार बच्चे पर अपना चयन थोपते हैं, तो बच्चा धीरे-धीरे अपनी असली पसंद और इच्छाओं से दूर हो जाता है। यदि व्यक्ति वयस्क होने के बाद भी दूसरों के फैसलों के अनुसार जीवन जीता है - जैसे कि ऐसी किसी पेशेवर दिशा में काम करना जो उसे वास्तव में पसंद नहीं है - तो उसमें इम्पोस्टर सिंड्रोम विकसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ में लगे होते हैं जिसे आपने खुद नहीं चुना, तो उसमें संतुष्टि और आत्मविश्वास महसूस करना मुश्किल होता है।
-
अत्यधिक अपेक्षाएँ: जब माता-पिता अक्सर ऐसे वाक्य कहते हैं जैसे: "हाँ, आपने अच्छा किया, लेकिन इससे और बेहतर हो सकता था" - उदाहरण के लिए, "99 अंक क्यों आए, 100 क्यों नहीं?" या "गोल्ड मेडल मिला? दो मेडल क्यों नहीं?" - तो इससे बच्चे के भीतर खुद के प्रति अवास्तविक और अत्यधिक मांगें विकसित हो जाती हैं। ऐसे लक्ष्य जो व्यावहारिक रूप से पूरे कर पाना संभव नहीं होते। इसका नतीजा यह होता है कि व्यक्ति लगातार खुद से असंतुष्ट रहता है और हमेशा आत्म-संदेह की स्थिति में जीता है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न कर ले।
-
सफलताओं के नकारात्मक नतीजे: यदि किसी व्यक्ति की सफलता के कारण उसे अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ा हो, जैसे कि दूसरों द्वारा मज़ाक उड़ाना, बड़ों की उपेक्षा, प्रतिद्वंद्वियों की ओर से अपमान आदि, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस वजह से व्यक्ति के मन में एक विकृत संबंध बन जाता है - "सफलता = कष्ट"। इससे वह अपनी सफलताओं और कौशल को स्वीकार करने से इनकार करने लगता है, ताकि वह खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके।
वयस्क उम्र में इम्पोस्टर सिंड्रोम निम्नलिखित कारणों या सोच की आदतों के प्रभाव से पैदा होता है और बढ़ जाता है:
-
आत्म-प्रतिबिंब की कमी: व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने और उनको नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता, यह नहीं जान पाता कि वह कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा क्यों महसूस करता है। उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म-नियंत्रण का स्तर सामान्य से कम होता है।
-
कमज़ोर फीडबैक कल्चर: व्यक्ति को सहयोगियों या वरिष्ठों से फीडबैक प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते या वह उनका उपयोग नहीं करता। इसलिए उसे अपने काम के मूल्यांकन के लिए केवल खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कि अक्सर बहुत ही व्यक्तिगत और कम आकलन वाला होता है।
-
स्पष्ट KPI और पारदर्शी रिवॉर्ड प्रणाली का अभाव: यदि व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि अपनी उपलब्धियों को कैसे मापें और कैसा उनका मूल्यांकन करें, लेकिन वह देखता है कि कोई दूसरा कर्मचारी, जिसकी प्रेजेंटेशन समान लगती है, प्रमोशन या बोनस प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में आत्म-मूल्यांकन और आत्म-संदेह की समस्या पैदा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नियमित फीडबैक और पारदर्शी रिवॉर्ड प्रणाली इस कारक के आत्म-सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करती है।
-
अत्यधिक लम्बा टीमवर्क: टीम में काम करते समय व्यक्ति अपने व्यक्तिगत योगदान का सही आकलन नहीं कर पाता और सफलता को पूरे समूह के साथ साझा करता है, जिससे उसकी अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत महत्वपूर्णता का एहसास कम हो जाता है। इसलिए, सलाह दी जाती है, कि टिमवर्क के साथ-साथ व्यक्तिगत या स्वतंत्र परियोजनाओं (यहां तक कि छोटे पैमाने पर) को भी समय-समय पर अपने जीवन में शामिल करना चाहिए।
इसके अलावा, कई विशेषज्ञों के अनुसार, इम्पोस्टर सिंड्रोम उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनका व्यक्तित्व, न्यूरोटिक प्रकार का होता है, यानी जो मूल रूप से न्यूरोसिस (मनोवैज्ञानिक अस्थिरता) के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और जिनकी मानसिकता ज़्यादा लचीली या अस्थिर होती है। ऐसे लोगों में इम्पोस्टर सिंड्रोम अचानक पैदा हो सकता है, खासकर जब उन्हें अचानक फीडबैक में बदलाव का सामना करना पड़े, नौकरी बदलनी पड़े, वित्तीय संकट आए, या अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे कि जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर से उनका सामना हों।
पिछले कुछ सालों में इम्पोस्टर सिंड्रोम के फैलाव के पीछे सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। सोशल मीडिया अक्सर "सफलता की चमक-धमक" दिखाता है, लेकिन सफलता पाने की प्रक्रिया में होने वाली गलतियों और मुश्किलों को नजरअंदाज करता है। जब हम दूसरों की आदर्श जीवनशैली देखते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हम "पर्याप्त सफल नहीं हैं"। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी खुद की उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय उनसे शर्म महसूस करने लगते हैं।
इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के प्रकार

आंकड़ों के अनुसार, हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार इम्पोस्टर सिंड्रोम का अनुभव करता है। हालांकि इसके लक्षणों में समानता होती है और यह एक स्पष्ट अवधारणा लगती है, लेकिन "इम्पोस्टर" वास्तव में अलग-अलग प्रकार के होते हैं। इसी संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक वैलेरी यंग ने इम्पोस्टर सिंड्रोम के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं:
-
परफेक्शनिस्ट: अत्यधिक और अस्वस्थ लगाव ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम पाने के लिए, जहाँ व्यक्ति हर काम को पूरी तरह सही और त्रुटिरहित करने पर ज़ोर देता है। कोई भी छोटी गलती या कमी होने पर वह व्यक्ति पूरी मेहनत से किया गया काम दोबारा करने लगता है, जिससे उसे काम की सफलता का संतोष नहीं होता और वह काम के सकारात्मक पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है।
-
विशेषज्ञ: यह ज्ञान की पूर्णता और कौशल की परिपूर्णता पर केंद्रित होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा से निपटना कठिन पाता है, खासकर तब जब उसे अपनी राय दूसरों से टकरानी पड़ती है या जब यह पता चलता है कि उसके पास वर्तमान में आवश्यक अनुभव की कमी है। ऐसे मामलों में वह व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकता है और तुरंत ही सीखने पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, लेकिन यह सीखना अक्सर थका देने वाला और मानसिक रूप से तनावपूर्ण होता है।
-
सोलो: इस प्रकार के व्यक्ति में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता होती है, वह अपने काम दूसरों को सौंपने या मदद मांगने में असमर्थ होता है, चाहे उसे कितनी भी ज़रूरत हो। बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करना उसके लिए अपनी अक्षमता को स्वीकार करने के समान होता है।
-
प्रतिभाशाली: यह व्यक्ति काम को सरलता और तेजी से पूरा करने पर ज़ोर देता है। जैसे ही किसी काम में मेहनत करनी पड़ती है या वह काम पहली बार में सही तरीके से नहीं होता, तो वह खुद की कड़ी आलोचना करने लगता है, शर्म महसूस करता है और इसे असफलता के बराबर मानता है।
-
अलौकिक: इस प्रकार का व्यक्ति एक साथ कई क्षेत्रों में खुद को सिद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन हर क्षेत्र में उसे आत्म-संदेह और असंतोष का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह किसी दूसरे क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करता है (या उसे अपनी सूची में जोड़ लेता है), लेकिन असंतोष की स्थिति फिर से दोहराई जाती है।
संकेत और लक्षण
ऐसा लगता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम को पहचानना आसान है, लेकिन अक्सर लोग खुद में इसके होने का अंदाजा भी नहीं लगा पाते, क्योंकि यह सिंड्रोम परफेक्शनिज्म (जो इसके एक उपप्रकार और विशेषता भी है) से काफी मिलता-जुलता होता है। अलग-अलग लोगों में इम्पोस्टर सिंड्रोम के लक्षण वास्तव में बहुत अलग-अलग तरीके से प्रकट होते हैं। यह केवल करियर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में और खासकर दूसरों के साथ संबंध बनाने में भी यह प्रभाव दिखा सकता है।
सामान्य लक्षण
-
यह मानना कि आपने जो कुछ भी अभी तक हासिल किया है, वह केवल भाग्य और संयोग की वजह से है, न कि आपके कौशल और मेहनत के कारण।
-
आपका आत्म-सम्मान आपकी कार्यक्षमता और वर्तमान कौशल के मूल्यांकन पर निर्भर करती है (उदाहरण के लिए, यदि आप पिछले दो हफ्ते आराम कर रहे थे और कुछ नहीं किया या किसी नए प्रोजेक्ट में असफल हुए, तो आपके आत्म-सम्मान में अचानक गिरावट आती है)।
-
संतोष पाने के लिए अत्यधिक मेहनत करना जरूरी समझना, यानी बिना कड़ी मेहनत के आपको संतुष्टि महसूस नहीं होती।
-
समर्पण और पूरी तरह से किसी विचार या उद्देश्य को अपना सब कुछ समर्पित कर देना, भले ही इससे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य, को नुकसान हो।
-
अकेलेपन और समाज से अलगाव का अनुभव, यह महसूस करना कि वास्तव में आपकी कद्र नहीं की जाती और आपको गंभीरता से नहीं लिया जाता।
-
डिप्रेसिव एपिसोड (मनोवैज्ञानिक अवसाद के क्षण), बढ़ी हुई चिंता और अन्य मानसिक विकारों का होना।
-
आक्रामकता या डर, उन परिस्थितियों में जब आपको अपनी बात को साबित करना होता है, क्योंकि आपको डर होता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी अक्षमता और कमजोरी को जान जाएगा।
काम पर
करियर निर्माण और कार्यस्थल पर इंपोस्टर सिंड्रोम कुछ इस प्रकार सामने आ सकता है:
-
नई और अनजानी जिम्मेदारियों को निभाने का डर।
-
किए गए काम से असंतोष।
-
सबसे छोटी गलती पर अपनी उपलब्धियों को नकारना और खुद को बेकार समझना।
-
अत्यधिक प्रतिस्पर्धा जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को खत्म कर देती है।
-
नौकरी छूटने का डर और काम का अत्यधिक जुनून, देर तक काम पर रहने की आदत, लगातार ओवरटाइम करना।
-
खुद का लगातार मूल्यांकन करना और दूसरों से तुलना करना (अक्सर अपने पक्ष में नहीं)।
-
हर काम या प्रोजेक्ट के लिए अत्यधिक तैयारी करना, जो बहुत लंबा खिंच जाती है और थकावट का कारण बनती है।
-
तारीफ मिलने पर "यह तो कोई बात नहीं" कहना और अपनी उपलब्धियों को नकारना जब दूसरे लोग उन्हें नोटिस करते हैं और उनकी सराहना करते हैं।
-
ऐसी स्थितियों को सहन करना जब आपकी उपलब्धियों का श्रेय किसी और को दिया जाता है या पूरी टीम में बाँट दिया जाता है (ऐसे में व्यक्ति नाराज नहीं होता और स्पष्ट अन्याय को अनदेखा करता है)।
-
उच्च सफलता प्राप्त करने पर अपराधबोध और शर्म महसूस करना, जैसे कि सहकर्मियों के सामने शर्मिंदगी होना क्योंकि आपने कुछ बेहतर किया या आपकी ज्यादा तारीफ हुई, जिससे आप सहकर्मियों और टीम से दूरी बना लेते हैं या सफलता का श्रेय उन लोगों को दे देते हैं जिनका इसमें असल में कोई संबंध नहीं होता।
संबंधों में
सामान्य धारणा के विपरीत कि इम्पोस्टर सिंड्रोम केवल कार्यस्थल में होता है, वास्तव में यह व्यक्तिगत संबंधों में भी प्रकट हो सकता है, खासकर रोमांटिक या दोस्ताना संबंधों में। यहाँ इसके लक्षण काफी हद तक ऊपर बताए गए लक्षणों से मेल खाते हैं और कुछ हद तक अलग-अलग हैं:
-
अपने में कमी महसूस करना। यह इस तरह प्रकट हो सकता है कि आपको बार-बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपका प्रिय व्यक्ति आपसे बेहतर किसी और को खोज सकता है और एक दिन निश्चित ही ऐसा करेगा। आप उसे बहुत ऊँचा स्थान देते हैं, जबकि खुद को छोटा आंकते हैं और लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, चाहे वह आपके साथी के पसंदीदा सेलिब्रिटी हों या उसके दोस्त।
-
कमियों पर ध्यान केंद्रित करना। आप हमेशा अपनी छोटी-मोटी कमियों पर ध्यान देते हैं: जैसे नाक पर उभरा पिंपल; अपने वजन को बार-बार नापना या खुद को शीशे में देखना; खुद को डांटना कि खाना स्वादिष्ट या विविध नहीं बना, आदि।
-
विश्वासघात का डर। इम्पोस्टर सिंड्रोम में यह बिना किसी आधार की पैथोलॉजिकल जलन नहीं होती जो लड़ाई-झगड़े का कारण बने, बल्कि यह चिंता और परेशान करने वाले विचार होते हैं कि आपका साथी वास्तव में आपको धोखा दे रहा है या जल्द ही ऐसा करने लगेगा। और इसके लिए केवल आप ही दोषी होंगे, क्योंकि आपका साथी बस यह समझ चुका है कि आप उसके लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं।
-
साथी के चुनाव को लेकर शंका। ये अक्सर इस रूप में प्रकट होती हैं कि "क्या मैंने अपने जीवन के लिए सही व्यक्ति चुना है?", जबकि असल में यह डर होता है कि एक दिन आपका साथी भी आपसे यही सवाल करेगा। इससे अचेतन रूप से भविष्य के दर्द से बचने या "साथी को आपसे बेहतर किसी और को खोजने देने" की इच्छा के कारण अनावश्यक अलगाव हो सकता है।
-
बुरे की उम्मीदें। आप हमेशा तनाव में रहते हैं कि आपका साथी आपसे नाराज होगा, देर से आएगा, भूल जाएगा, वापस कॉल नहीं करेगा, आपकी मेहनत की कद्र नहीं करेगा, आदि।
इसके परिणामस्वरूप, यह न केवल पहले से बने रिश्तों को खराब कर सकता है, बल्कि नए संबंध बनाने में भी बाधा डाल सकता है, क्योंकि जब एक साथी में लगातार आत्म-संदेह होता है तो मजबूत संबंध स्थापित करना संभव नहीं होता। यह भावनाओं के प्रकट होने में भी बाधा डाल सकता है और संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है, उदाहरण के लिए, जब साथी खोने या धोखे खाने का डर एक साथी को बार-बार इस विषय को उठाने और जलन दिखाने के लिए मजबूर करता है। अक्सर, व्यक्तिगत संबंधों में इम्पोस्टर सिंड्रोम इस हद तक जाता है कि व्यक्ति जानबूझकर साथी और परिस्थितियों को उकसाता है, जो उसकी चिंताओं को साबित कर दें, ताकि रिश्ते तोड़ना आसान हो जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि कार्यस्थल में ऐसा लक्षण बहुत कम देखा जाता है; आमतौर पर यह उल्टा होता है और नौकरी खोने के डर और काम के प्रति अत्यधिक लगाव के रूप में बदल जाता है, जो इस जोखिम को कम करने की कोशिश होती है।
इम्पोस्टर सिंड्रोम टेस्ट

यह कैसे समझें कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है? इंटरनेट पर आप कई तरह के टेस्ट पा सकते हैं, जो यह पता लगाने में मदद करते हैं कि कहीं आप इस स्थिति से तो नहीं जूझ रहे। सबसे लोकप्रिय टेस्टों में से एक है पॉलीन क्लैंस द्वारा विकसित टेस्ट, जिसमें कई कथन दिए गए होते हैं, और आपको हर एक के लिए "हाँ" या "नहीं" में उत्तर देना होता है और कि क्या यह कथन आपके ऊपर लागू होता है या नहीं। कुछ विशेषज्ञ इन बिंदुओं की सूची को और भी विस्तृत करते हैं। नीचे हम आपको ऐसे ही कुछ कथनों से अवगत करा रहे हैं, जिनकी मदद से आप यह पहचान सकते हैं कि क्या आप भी इस मानसिक स्थिति से प्रभावित हैं, या नहीं।
-
आपको लगता है कि आपकी मौजूदा सफलता और स्थिति केवल किस्मत या दूसरों की मदद की वजह से है।
-
आप मानते हैं कि जो कुछ आपने हासिल किया है, वह कोई भी आम व्यक्ति हासिल कर सकता है।
-
आप अपनी छोटी-छोटी गलतियों के लिए खुद को ज़्यादा और लंबे समय तक दोषी मानते हैं, जबकि आपके जानने वाले लोग ऐसा नहीं करते।
-
आप अक्सर कई प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे।
-
आपको अपने आस-पास के लोगों के सामने अपराधबोध महसूस होता है, मानो आप उनके द्वारा आपके बारे में बनाए गए विचारों को धोखा दे रहे हों।
-
आप अक्सर अपनी सेवाओं की कीमत बहुत कम लगाते हैं या बिना पैसे के काम करने को तैयार हो जाते हैं।
-
आपको किसी खास क्षेत्र में खुद को विशेषज्ञ के रूप में पेश करना मुश्किल लगता है।
-
आपको लगता है कि आपके आस-पास के ज़्यादातर लोग आपसे ज़्यादा समझदार, प्रतिभाशाली और सक्षम हैं।
-
आप अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और हमेशा खुद को कम आकते हैं।
-
कभी-कभी (और शायद अभी भी) आप सोचते हैं: क्या हो अगर मुझे कोई "सिंड्रोम" नहीं है, और मैं सच में एक धोखेबाज़ हूँ?
अब यह आंकलन करें कि आपने कितने कथनों का जवाब "हाँ" में दिया, और हर "हाँ" के लिए एक अंक जोड़ें। यदि आपके पास:
-
3-4 अंक - हाँ, आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है, लेकिन यह काफी हल्का है और आपकी ज़िंदगी या मानसिक स्थिति पर ज्यादा असर नहीं डालता। आप इसे आसानी से पहचानकर दूर कर सकते हैं।
-
5-8 अंक - आपके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम मध्यम स्तर पर मौजूद है, और यह आपके काम और रिश्तों को प्रभावित कर रहा है।
-
8 से ज़्यादा अंक - आपके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत गहराई से बैठा हुआ है, जो आपकी व्यक्तित्व में नकारात्मक बदलाव ला सकता है और करियर व निजी जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे जल्द से जल्द निपटना जरूरी है! अगर स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, तो किसी विशेषज्ञ की मदद लेना भी आवश्यक हो सकता है।
इम्पोस्टर सिंड्रोम से कैसे लड़ें

इम्पोस्टर सिंड्रोम से कैसे लड़ें? असल ज़िंदगी में यह इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपको हर दिन इस एहसास से जूझना पड़ता है कि आप जिस जगह पर हैं, वो आपकी असली काबिलियत की वजह से नहीं है - और आप कभी भी उस ऊंचाई से नीचे गिर सकते हैं। कभी-कभी, इस मानसिक स्थिति को पूरी तरह से समझने और उससे बाहर आने के लिए (खासकर जब यह बहुत गहराई से बैठा हो), आपको एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ - जैसे कि साइकोथेरेपिस्ट या मनोवैज्ञानिक - की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि, कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें आप खुद आज़मा सकते हैं, और ये भी इस सिंड्रोम को हराने और इससे बाहर आने में आपकी मदद कर सकते हैं।
तरीका 1: खुद की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अतीत के "खुद" से करें
असल में, यही तुलना करने का सबसे स्वस्थ और सकारात्मक तरीका माना जाता है - और इसे बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करना बेकार है, क्योंकि हर इंसान पर अलग-अलग बाहरी परिस्थितियाँ असर डालती हैं और हर व्यक्ति के अंदर गहरे (यहाँ तक कि जैविक!) स्तर पर भी भारी अंतर होते हैं। अगर अब तक आपने इस आदत को विकसित नहीं किया है, तो अभी से इसे अपनाना शुरू करें। इसके लिए आप प्लानर और road map की मदद ले सकते हैं, जैसे कि:
-
यह आंकलन करें कि आप एक साल पहले कहाँ थे - अपने करियर या निजी जीवन में किस स्थिति में थे? उस समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? क्या आपने उनसे पार पा लिया? कैसे?
-
अब अपने मौजूदा कौशल और उपलब्धियों की तुलना एक साल पहले के अपने कौशल और उपलब्धियों से करें। सोचें कि इस दौरान आपने क्या-क्या नया सीखा? कौन-कौन सा अनुभव प्राप्त किया? आपने अपने व्यवहार, काम या रिश्तों में क्या बदलाव किए?
-
अपने पिछले अनुभव की तुलना मौजूदा अनुभव से करें। खुद की एक साल पहले की स्थिति को इस तरह देखें जैसे आप दो अलग-अलग व्यक्ति हों। अब सोचें - यह तुलना किसके पक्ष में जाती है?
-
आगे का road map तैयार करें। अब यह तय करें कि आप एक साल बाद खुद को किस स्थिति में देखना चाहते हैं। लिखें कि आपको इस समय तक कौन-कौन से कौशल सीखने हैं, किस पद पर होना है, कहाँ रहना है, कौन-सी आदतें अपनानी हैं आदि। साथ ही यह भी सोचें कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। अब यह आपका लक्ष्य है, और एक साल बाद आप खुद की तुलना इसी लक्ष्य से कर सकते हैं ताकि जान सकें कि आपने इसे हासिल किया है या नहीं।
तरीका 2: अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता बढ़ाएँ
अनिश्चितता सहन करने की क्षमता का मतलब है कि आप उस अनिश्चितता और अप्रत्याशित परिस्थितियों को बगैर ज़्यादा तनाव या नियंत्रण की जरूरत महसूस किए सह सकें, जब ऐसी परिस्थितियाँ आएं जो आपके नियंत्रण से बाहर हों या भविष्य अस्पष्ट हो। अपनी इस क्षमता को बढ़ाने के कुछ सरल और कम कष्टदायक तरीके हैं, जैसे कि:
-
हफ्ते में एक बार अपने ऑफिस या घर जाने के रास्ते को बदलें और ऐसी नई, अपरिचित सड़क पर जाएं जिसे आपने पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया हो।
-
कैफे में ऐसे व्यंजन ऑर्डर करें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं चखा हो।
-
किसी रेस्टोरेंट में जाने से पहले मेन्यू पढ़ें नहीं, या फिर बिना मेन्यू देखे नए जगह पर जाकर भोजन करें।
-
अपने सप्ताहांत या काम की योजना न बनाएं - लेकिन यह केवल सप्ताह में एक दिन ही करें! योजना बनाना निश्चित रूप से हमें ज़्यादा प्रभावी बनाता है, लेकिन कभी-कभी अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए इसे थोड़ा त्यागना भी जरूरी होता है।
अनिश्चितता सहन करने की ज़्यादा क्षमता हमें अपनी गलतियों को आसानी से सहन करने में भी मदद करती है, क्योंकि इम्पोस्टर सिंड्रोम अक्सर इस डर से जुड़ा होता है कि हम नियंत्रण खो देंगे और इस वजह से किसी के सामने बेनकाब हो जाएंगे। यह समझना कि दुनिया में कोई बड़ी आपदा नहीं होती जब आप सहज रूप से कुछ नया करते हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और प्रयोग करते हैं, आपकी आत्म-संदेह की भावना को कम करने में मदद करेगा।
तरीका 3: नियमित फीडबैक माँगें
अगर आपको यह चिंता सताती है कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की या आपने पर्याप्त अच्छा परिणाम हासिल नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में अपने विश्वसनीय और सम्मानित लोगों की राय पर भरोसा करना, अपनी आदत बनाएं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे एक और जुनून न बनने दें और इसके लिए एक सख्त समय-सारणी बनाएं। उदाहरण के लिए, महीने में एक बार या किसी प्रोजेक्ट के खत्म होने पर उनसे फीडबैक और प्रदर्शन का मूल्यांकन माँगना। यह भी ध्यान रखें कि फीडबैक देने वाला व्यक्ति आपके लिए सम्मानित और विश्वसनीय होना चाहिए। यदि आप उस व्यक्ति की राय पर विश्वास नहीं करेंगे और बार-बार खुद में कमियां ढूंढ़ने लगेंगे, भले ही आपको बताया गया हो कि आपने काम बहुत अच्छा किया है, तो यह तरीका बेकार साबित होगा।
यह नियम बनाएं कि आप तब ही अपनी गलतियों को लेकर चिंतित होंगे और उन्हें सुधारेंगे जब कोई आपको वे गलतियाँ बताए। अगर कोई आपसे आपके काम की गुणवत्ता के बारे में पूछे और आपको कहे कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब सच में सब कुछ ठीक है। इसके अलावा, उन लोगों के उदाहरण अपने सामने रखें जो सफलतापूर्वक इम्पोस्टर सिंड्रोम से निपटते हैं या जिन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि वे दूसरों से कमतर हैं। उनसे बातचीत करें और उनसे कुछ सुझाव माँगें!
तरीका 4: अपने अंदर के आलोचक से बहस करें और अपने भीतर एक स्वस्थ वयस्क को विकसित करें
स्कीमा थैरेपी के अनुसार, हम में कई अलग-अलग "मोड" या व्यक्तित्व एक साथ मौजूद होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो, हमारे अंदर कई अलग-अलग पक्ष होते हैं-कुछ मजबूत होते हैं, तो कुछ दबे हुए। उदाहरण के तौर पर, हर किसी के अंदर एक "भीतरी बच्चा" होता है, यह सच है। इसके अलावा, हमारे अंदर एक "भीतरी आलोचक" भी होता है और एक ऐसा पक्ष भी होता है जिसे हम "स्वस्थ वयस्क" कहते हैं। आप शायद समझ ही गए होंगे कि ये अलग-अलग पक्ष क्या काम करते हैं, है ना?
भीतरी आलोचक वह नकारात्मक आवाज़ है जो हमें बताती है कि हमने काम ठीक से नहीं किया, हम पूरी मेहनत नहीं कर रहे, हम तारीफ या प्यार के हकदार नहीं हैं, आदि। वहीं, "स्वस्थ वयस्क" हमारे अंदर वह अंदरूनी माता-पिता जैसा पक्ष है जो हमें सांत्वना देता है, हमारा समर्थन करता है और हमारी प्रशंसा करता है। स्वस्थ वयस्क को आलोचक से कई गुना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम में यह स्थिति उल्टी होती है - आलोचक ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मनोविज्ञान में आलोचक को दबाने के लिए कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे कि "कुर्सी तकनीक": आप अपने आलोचक को कल्पनात्मक रूप से अपने से दूर बैठा देते हैं, उसे एक नाम देते हैं, अगर चाहें तो उसकी कल्पना करते हैं, फिर उसके हर नकारात्मक बयान पर बहस करते हैं और खुद की रक्षा करते हैं जैसे कि आप किसी करीबी दोस्त की करते। स्वस्थ वयस्क को विकसित करने के लिए ख़ुद की देखभाल और अपने आप से सकारात्मक बातचीत बहुत जरूरी है, जैसे कि जब आप खुद से कहते हैं कि आपने पूरी कोशिश की है, आप कुछ अच्छा पाने के हकदार हैं, छोटी-छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए, आदि। कुर्सी तकनीक के समान एक तरीका यह भी है कि आप एक नरम खिलौना लेकर उसे बच्चे की तरह सांत्वना दें। बच्चों के साथ बातचीत करना और शिक्षक, पालक या मार्गदर्शक की भूमिका निभाना भी इस प्रक्रिया में मदद करता है।
तरीका 5: अपनी भावनात्मक आत्म-नियमन की क्षमता बढ़ाएँ
अक्सर हमें गलतियाँ नहीं, बल्कि अपनी ही प्रतिक्रियाएँ और उन पर महसूस होने वाली भावनाएँ डराती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको असफलता के समय अपनी भावनाओं को समझना मुश्किल लगता है, तो आप उस स्थिति से डर सकते हैं क्योंकि वह आपको अजनबी और नियंत्रित न होने वाली लगती है। ऐसा ही तब होता है जब आपको तारीफ़ मिलती है। खुद से पूछें कि उस समय आप क्या महसूस करते हैं? गर्व? और क्या गर्व आपको डराता है? शायद खुशी के पल आपको आराम महसूस कराते हैं, और आराम आपको कमजोर या असुरक्षित महसूस कराता है। या फिर बचपन में आपको यह सिखाया गया हो कि "अच्छे कामों पर गर्व नहीं करना चाहिए, वह तो बस सामान्य बात है।"
अपनी भावनात्मक ट्रिगर्स को बेहतर तरीके से समझने और नई या अप्रत्याशित भावनाओं तथा उन्हें न संभाल पाने के डर से बचने के लिए, एक भावना डायरी बनाएं। दिन में 2-3 बार (जैसे अलार्म बजने पर) यह नोट करें कि उस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, उस भावना के पैदा होने का कारण क्या था, और इन भावनाओं के शारीरिक लक्षण क्या हैं, जैसे हाथों में कंपकंपी, सीने में गर्माहट आदि। आजकल मोबाइल फोन के लिए विशेष ऐप्स भी उपलब्ध हैं, जैसे कि Daylio, जो इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं।
तरीका 6: अपनी उम्मीदें कम करें
इस बात पर आप भी सहमत होंगे, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से 50 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, जो जीवन में कभी दोड़ा ही नहीं। तो फिर आप खुद से 100% परफॉर्मेंस की उम्मीद क्यों करते हैं, खासकर जब आप उस काम या टूल से पहली बार रूबरू हो रहे हों? या जब आपका काम पर केवल दूसरा या तीसरा दिन हो? इंसान के लिए एडाप्टेशन, बीमार होना, खराब सेहत और जीवन के अन्य क्षेत्रों की समस्याएं जैसी स्वाभाविक अवस्थाएं होती हैं - ये सब प्रभावकारिता पर असर डालती हैं, और यह बिलकुल सामान्य है। अपने आप से और दूसरों से अपनी उम्मीदों की तुलना करें: क्या आप अपने दोस्त के प्रति भी ऐसी सख्त उम्मीदें रखेंगे, जब वह इसी स्थिति में हो?
अपेक्षाओं को कम करना निजी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई होटल चुनने से पहले 1000 विकल्पों को खंगालने की आदत है (भले ही आप वहां सिर्फ़ 2 दिन ठहरने वाले हों), तो अपनी अपेक्षाओं की सूची को घटाकर केवल 2-3 मुख्य मानदंडों तक सीमित करें - जैसे कि "मेट्रो के पास हो" और "नाश्ता शामिल हो"।
निष्कर्ष
इम्पोस्टर सिंड्रोम आज की दुनिया में एक तरह से सामान्य स्थिति बन चुका है, जब हम हर तरफ़ दूसरों की सफलता की कहानियों और कार्यक्षमता बढ़ाने वाले ट्रेनिंग्स से घिरे रहते हैं। हालाँकि ऐसा माना जाता है कि इसका हम पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है - क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जो इस सिंड्रोम से जूझते हैं, असाधारण ऊँचाइयाँ छू लेते हैं, क्योंकि यह उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है - फिर भी यह एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है। इससे जूझते हुए, अपने आस-पास मौजूद लोगों को मत भूलिए - ज़्यादातर लोग आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे, जब वे आपकी स्थिति के बारे में जानेंगे, चाहे वह आपका कोई सहकर्मी हो या जीवन साथी। इम्पोस्टर सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, और आप निश्चित रूप से इससे उबर सकते हैं!